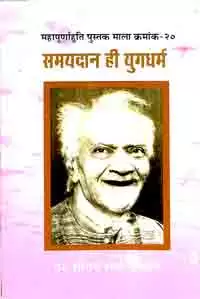|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> समयदान ही युगधर्म समयदान ही युगधर्मश्रीराम शर्मा आचार्य
|
|
||||||
प्रतिभादान-समयदान से ही संभव है
7
प्रामाणिकता और प्रखरता ही सर्वत्र अभीष्ट
आज की परिस्थितियों पर सामयिक विचार-मंथन का निष्कर्ष एक ही है, कि हम सब भ्रांतियों के युग में रह रहे हैं और मानवी गरिमा के अनुरूप मर्यादा परिपालन में भटक गए हैं। सुधार इन दोनों का ही बन पड़े, तो समझना चाहिए कि उपाय का अवलंबन मिल गया, जो युग समस्याओं का समाधान कर सकने में पूरी तरह समर्थ है। इस उपाय को क्रियान्वित करके कौन दिखाए, इस संदर्भ में आशा की सुई उन वरिष्ठ प्रतिभाओं पर जाकर रुकती है, जो समयदान के रूप में अपने परम पुरुषार्थ का प्रस्तुतीकरण कर सकें। यह समयदान आलसियों प्रमादियों जैसा नहीं, वरन उसके साथ कठोर श्रम और भाव-संवेदनाओं का गहरा पुट घुला मिला रहना चाहिए।
यह किनसे बन पडेगा ? उसका उत्तर महाकाल के शब्दों में ही मिल जाता है जो अपने को तपे सोना जैसा खरा सिद्ध कर सके। चिंतन, चरित्र और व्यवहार की तीनों जॉच-पड़तालों में भली प्रकार उत्तीर्ण हो सके।" यह कार्य अति सरल भी है और अति कठिन भी। सरल उनके लिए जो जीवन को एक बहुमूल्य दैवी अनुकंपा मानते हैं और उनके श्रेष्ठतम उपयोग की बात सोचते हैं। कठिन उनके लिए जिन पर वासना, तृष्णा और अहंता की तिकड़ी पूरे जोर-शोर के साथ हावी है।
भव-बंधनों में बाँधने वाली तीन जंजीरें प्रख्यात हैं। उनका उल्लेख कहीं लोभ, मोह, अहंकार के रूप में किया गया है, कहीं इनकी गणना तृष्णा, वासना और अहंता के नाम से कराई गई है। दोनों ही प्रतिपादन एक ही तथ्य को अलग-अलग शब्दों में व्यक्त करते हैं। प्रथम बंधन लोभ-तृष्णा के प्रभाव से व्यक्ति में धन बटोरने की ललक चढी रहती है। इसके साथ वह अनाचार तक करता है। और उसके प्रभाव से खिंचते चले आने वाले दुर्व्यसनों का शिकार बनता है। इससे लौकिक और पारलौकिक दोनों ही स्तर के चित्र-विचित्र अनर्थ खड़े होते हैं। औसत नागरिक स्तर का निर्वाह किसी के लिए कठिन नहीं है। वह कुछ ही घंटों के परिश्रम से जुट जाता है और शेष समय का सदुपयोग पुण्य परमार्थ जैसे दिव्य प्रयोजनों में ही हो सकता है।
संग्रहीत संपत्ति को बेचकर बैंक में डाल देने से भी उसका ब्याज पाने की कितने ही लोग व्यवस्था बना लेते हैं, ताकि घर खर्च आसानी से चल सके। पूर्व काल में घर के अन्य कमाऊ लोग परिवार का एक सदस्य परमार्थ के लिए समर्पित करके अपनी गौरव भरी परंपरा चलाते रहते थे। सतयुग के ब्राह्मण परिवार में से एक सदस्य परिव्राजक की तरह भ्रमणशील सेवा साधना में निरत रहता था। आज भी चिंतन को थोड़ा झकझोरा जा सके तो वैसी ही व्यवस्था फिर नए सिरे से बन सकती है।
दूसरा भव-बंधन है जिसका तात्पर्य है स्त्री-बच्चों का आश्रित परिवार इतना बड़ा और भारी बना लेना, जिसका भार निरंतर जुटे रहने पर ही किसी प्रकार उठाया जाना संभव हो सके। ऐसे लोग मनोरंजन के रूप में कुछ परमार्थ कर सकते हैं। पति-पत्नी तभी एक और एक मिलाकर ग्यारह बनते हैं, जब उच्च उद्देश्यों के लिए एक-दूसरे के सहयोगी बनें। संतान के दायित्व नहीं के बराबर बनाए रखें, अन्यथा उनका निर्वाह और अमीर बनने का मंसूबा, जीवन तत्त्व का सारा रस निचोड़ लेता है। वासना का प्रतिफल ही यह विषफल है। संतानरहित विवाहों में तो परमार्थ के लिए थोडी गुंजायश भी रहती है, पर यदि वह आकर्षण बढ़ता जाता है तो श्रम का नियोजन और मनोयोग उसी प्रयोजन में खप जाता है।
यदि परिवार को स्वावलंबी सुसंस्कारी भर बनाने तक का लक्ष्य सीमित रखा जाए, उस पर बड़प्पन थोपना अनिवार्य न समझा जाए, तो विवाह-बंधन नहीं बनता और न वह भार बनकर सिर पर लदता है। जो भी हो जिस प्रकार लोकसेवियों के लिए निर्वाह व्यय में कटौती करना आवश्यक है; वहाँ यह भी उचित है कि परिवार के उद्यान में रहकर दायित्वों के निर्वाह की शिक्षा तो प्राप्त करें, पर उसे हथकड़ी की तरह इतना कठोर न बना लें कि उसके अतिरिक्त और कुछ सोचना या करना बन ही न पड़े।
प्राचीन काल में लोकसेवियों को विशेषतया चिंतन और चरित्र के क्षेत्र में भावपरक उत्कृष्टता भरने वाले अध्यात्म प्रयास में निरत रहते देखा जाता था। वे ही देश की मान-मर्यादा को उच्च शिखर पर बनाए रखने का श्रेय संपादित करते रहते थे। इन दिनों आदर्शवादी आकांक्षाओं में बुरी तरह गिरावट आई है। अपनी जीवनचर्या से दूसरों को कारगर प्रकाश दे सकने वाले प्राणवान हूँढे नहीं मिलते। बकवादी तो पहले से भी अधिक बढ़ गए हैं, जो कथनी और करनी में भारी अतर रहने के कारण गदगी बिखेरते और अश्रद्धा का वातावरण बनाते देखे जाते हैं।
तीसरा व्यवधान है-अहंकार। समान स्तर के सज्जन व्यक्तियों को अपना आपा नम्रता से भरा-पूरा रखना चाहिए और दूसरों के साथ व्यवहार वार्तालाप इस स्तर पर करना चाहिए, जिसमें आदर सम्मान की भावना छलकती हो। अच्छे संबंध बनाए रखने का अपनत्व बढ़ाने का अवसर इसके बिना मिलता ही नहीं। अहंकारियों का रवैया ठीक इसका उलटा होता है। वे अपने बड़प्पन ढिंढोरा पीटते हैं। दूसरों की कमियाँ बताकर अपने को उन सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जिससे भी संपर्क साधा गया है, वह अपने को तिरस्कृत किया जा रहा अनुभव करता है और कहने वाले को अहंकार के दुर्गुण से घिरा हुआ मान लेता है। ऐसे लोग किसी का सच्चा स्नेहसम्मान भी नहीं पा सकते। अपना उल्लू सीधा करने वाले चापलूसों के अतिरिक्त और कोई न तो उनका मित्र होता है और न आड़े समय में काम आता है। देखा गया है कि अच्छी संस्थाओं में भी महत्त्वाकांक्षी बड़प्पन पाने के लिए लालायित लोग ही अनेकों विग्रह खड़े करते हैं एवं अन्ततः उस संगठन को ही बर्बाद कर देते हैं।
युग साधना में सफलता हेतु लोभ, मोह और अहंकार को जितना अधिक घटाया जा सकेगा, उतना ही स्तर इस योग्य बनता जाएगा कि लोग सच्चे मन से आदर भाव रखे और दिए गए परामर्श में अपना हित साधन समझे तथा स्वीकार करे।
इन दिनों सेवा क्षेत्र में करने योग्य तो अनेकानेक क्रिया कलाप हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा संपन्नता के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। सुविधा-संवर्धन के साधन जुटाना भी आवश्यक है। पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति उत्कृष्ट चिंतन का अभ्यासी बनने के साथ, अपनी समस्याओं का अपने बलबूते स्वयमेव हल खोज सके, स्वावलंबी बन सके। स्थायित्व इसी में है। अन्यथा दूसरों के साधन अनुदानों का आसरा तकते-तकते आंतरिक दृष्टि से भी दीन-हीन बन बैठेगा और देवताओं से लेकर श्रीमंतों के सामने गिड़गिड़ाकर कुछ प्राप्त कर लेने की तरकीबें ढूंढता रहेगा। स्वाभिमान और स्वावलंबन की दृष्टि से यह अनुपयुक्त ही है।
गुण, कर्म, स्वभाव, उत्कृष्टता ही वास्तविक सशक्तता है, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रामाणिक विश्वस्त एवं कर्तव्यपरायण समझा जाता है। वह जहाँ भी जाता है, वहीं सम्मान पाता है और समर्थन-सहयोग का वातावरण सहज ही बनता दीख पड़ता है।
इक्कीसवीं सदी के अवतरण में भगीरथ जैसे तपस्वी व्यक्तियों की आवश्यकता है। ऐसे तपस्वी जो मानवी सद्गुणों का अभ्यास करने के उपरांत देवोपम विशेषता के क्षेत्र में प्रवेश पा चुके हों। जो दूसरों के अवगुणों पर जीत पा लेता है, वह वीर कहलाता है, पर इससे भी अगली श्रेणी का 'महावीर' वह है जिसने आपको जीत लिया। ऐसे महामानव ही हनुमान स्तर के रीति-नीति अपनाते और आदर्शों के समुच्चय भगवान के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित रहकर, जन-जन की श्रद्धा के भाजन बनते हैं। दैवी अनुग्रह तो उन पर अजस्त्र रूप से बरसता ही है। यह धारणा ठीक है कि अपना पुरुषार्थ भी कम न था, पर उसे सफल बनाने के लिए अदृश्य लोक से जितने अनुदान बरसे, उनका महत्त्व भी कम करके नहीं आँका जा सकता।
खरे सोने की ही पूरी कीमत उठती है, भले ही उसे स्वर्ण विक्रेता की दुकान पर क्यों न ले जाया जाए ? खोटे सिक्के हर जगह दुत्कारे जाते हैं, उनकी असलियत तो अंध भिखारी भी अनुमान लगाने भर से जान लेता है। बड़े कामों के लिए बड़ी हस्तियाँ ही अभीष्ट होती हैं। इक्कीसवीं सदी के साथ एक से एक बढ़कर वजनदार और महत्त्वपूर्ण कार्य जुड़े हुए हैं। उन्हें संपन्न करने के लिए मनोबल के धनी और चरित्र बल से मूर्धन्य स्तर के व्यक्ति ही चाहिए। तलाश उन्हीं की हो रही है। प्रतिभा परिष्कार का अभियान इसी दृष्टि से चलाया जा रहा है। उस परिष्कार से तपकर निकले हुए व्यक्ति न केवल अपने में अग्रगामी वरिष्ठजनों में गिने जाने योग्य बनेंगे वरन् दूसरों को ऊँचा उठाने-आगे बढ़ाने में भी अपनी विशिष्टता का परिचय दे सकेंगे।
|
|||||
- दान और उसका औचित्य
- अवसर प्रमाद बरतने का है नहीं
- अभूतपूर्व अवसर जिसे चूका न जाए
- समयदान-महादान
- दृष्टिकोण बदले तो परिवर्तन में देर न लगे
- प्रभावोत्पादक समर्थता
- प्रामाणिकता और प्रखरता ही सर्वत्र अभीष्ट
- समय का एक बड़ा अंश, नवसृजन में लगे
- प्राणवान प्रतिभाएँ यह करेंगी
- अग्रदूत बनें, अवसर न चूकें


 i
i